आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्त्तिक पूर्णिमा तक चातुर्मास्य ब्रत विशेष
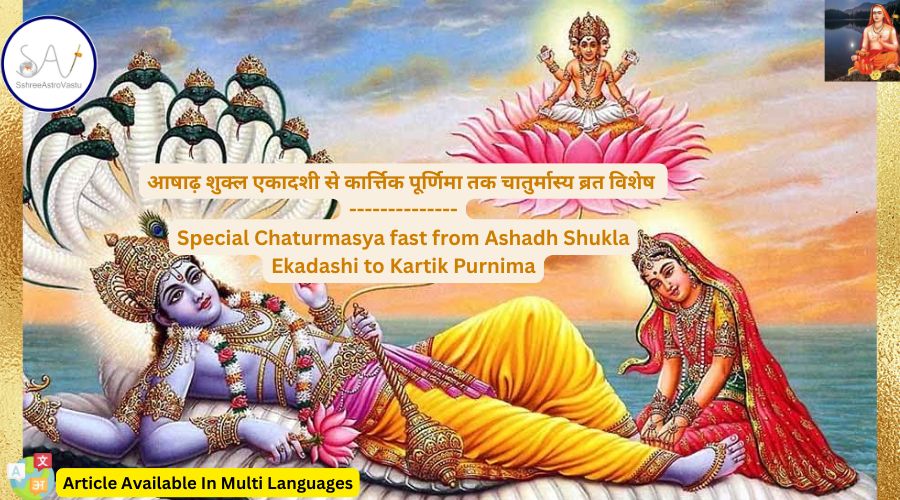
आषाढ़ शुक्ल पक्ष देव शयनी एकादशी के दिन उपवास करके मनुष्य भक्तिपूर्वक चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ करते हैं। एक हजार अश्वमेघ यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है, वही चातुर्मास्य व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है।।
अशुद्धि काल मान्यता युक्त इन चार महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, पत्तल पर भोजन, उपवास, मौन, जप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है – ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और महान फल देने वाला है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन और कुछ नहीं है। विशेषतः चतुर्मास में यह व्रत संसार में अधिक गुणकारक है।।
मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है। जो चतुर्मास में अपने प्रिय भोगों का श्रद्धा एवं प्रयत्नपूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएँ उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। अतः चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। ताम्बूल का त्याग करने से मनुष्य भोग- सामग्री से सम्पन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। नमक छोड़ने वाले के सभी पूर्तकर्म (परोपकार एवं धर्म सम्बन्धी कार्य) सफल होते हैं। जो मौनव्रत धारण करता है उसकी औचित्य पूर्ण आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता।।
चतुर्मास में काले एवं नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए। नीले वस्त्र को देखने से जो दोष लगता है, उसकी शुद्धि भगवान सूर्यनारायण के दर्शन से होती है। कुसुम्भ (लाल) रंग व केसर का भी त्याग कर देना चाहिए।।
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रीहरि के योगनिद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर ब्रत करनेवालों से अनेक भक्त अगले कार्तिक पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करते हैं। ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता और विमान प्राप्त करता है। बिना माँगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआँ बनवाने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर शहद का सेवन करता है, उसे महान पाप लगता है। चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करना चाहिए। जो प्राणियों की हिंसा त्याग कर द्रोह छोड़ देता है, वह भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है।।
चातुर्मास्य में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग करें। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है; यथा– “परनिंदा महापापं परनिंदा महाभयं। परनिंदा महद् दुःखं न तस्याः पातकं परम्।” अतः परनिंदा महान पाप है, परनिंदा महान भय है, परनिंदा महान दुख है और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। (स्कं. पु. ब्रा. चा. मा. 4.25)।।
चातुर्मास्य में वेदवित ब्रताचारिओं को ब्रताचारी- गृहस्थों ने भी यथाविधि सत्कार करने में पुण्य अर्जन होता है; यथा– “वेदविद्याव्रतस्नाताञ् श्रोत्रियान्गृहमेधिनः। पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्।” (मनु॰धर्मसूत्रम् ४/३१।।) अर्थात, “वेद पढ़े हुए ज्ञानी और ब्रह्मचर्य व्रत को पालने वाले ब्रताचारिओं को धर्म- पूर्वक गृहस्थ- जीवन पालन करने वाले आवश्यक पदार्थों द्वारा सत्कार करें। इनसे विरुद्ध लोगों का सत्कार न करें।।”
ब्रह्मचारियों को आवश्यक पदार्थ प्रदान कर सत्कार करने की मतलब, उनको हव्य- कव्य से सन्तुष्ट करना है। ’हव्य‘ का अर्थ है सामग्री जो होम में डाली जाती है। ’कव्य‘ का अर्थ है भोजन, रोटी, दाल, आदि जिनको पकाकर खाने के काम में लाते हैं। ’हव्य- कव्य‘ मुहावरे में भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं के नाम आते हैं।।
चातुर्मास्य में परिव्राजक साधु -संत- आचार्यों ने अपने मूल आश्रम या वास स्थान को लौट आते हैं और जप- तप- भजन- कीर्त्तन- शास्त्र मनन- मंथन रूप अध्यात्म- ज्ञानचर्चा में ये समय को अतिवाहित करते हैं। फिर शुद्ध काल आने से जनहित में जनपद को चले जाते हैं। ऐसे ही ऐश्वरीय कार्यक्रम था जगतगुरु शंकराचार्य जी का और आयुष अबधि कम होने से भी उनके द्वारा प्रतिष्ठित भारत के चार दिग में चार पवित्र धाम ही आजतक धर्म- संस्कृति रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाने की एक एक सफल अध्यात्म क्षेत्र का मान्यता को प्राप्त हुए हैं।।
ऐसे ज्ञान मनन- मंथन की तातपर्य भी श्रीमद्भागवत गीता में परिभाषित; यथा : “ऊर्ध्वमूलमधःशाख- मश्वत्थं प्राहुरव्ययं। छन्दांसि यस्य पर्णानि, यस्तं वेद स वेदवित।” इस पर विशद भावार्थ है– आदिपुरुष परमेश्वर- रूप ही ”मूलवाले” अर्थात, परमपिता परमेश्वर ही इस जगत का मूल आधार है। सबका आधार और सबसे श्रेष्ठ होने के कारण सबसे ऊपर है। परमेश्वर ही इस संसार बृक्ष का मूल होने से इसे “ऊर्ध्वमूल” वाला बृक्ष कहा जाता है और ब्रह्मरूप “मुख्य- शाखावाले”, अर्थात, आदिपुरुष परमपिता परमेश्वर से “उत्पत्तिवाला” होने के कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को उनसे “अधः”, अर्थात नीचे के स्थान वाला माना जाने से ब्रह्मा को नीचे की ओर “शाखावाला” काहा जाता है। संसार रूपी पीपल के बृक्ष को “अविनासी”, अर्थात इस बृक्ष का “मूल- कारण” परमात्मा अविनासी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है। इसलिए इस संसार बृक्ष को अविनासी कहा जाता है। वेद जिनके “पत्ते” है, अर्थात इस संसार बृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होनेवाली और यज्ञादिक कर्मो के द्वारा इस संसार बृक्ष की रक्षा और बृद्धि करनेवाले तथा शोभा बढ़ानेवाले होने के कारण वेद इस संसार बृक्ष के पत्ते कहे जाते है। — इस प्रकार इस संसार रूपी बृक्ष को जो मनुष्य मूल सहित तत्त्व से जानता है, वही वेद के तात्पर्य अर्थात भगवान की योगमाया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, कभी भी एक पल में टूट- जानेवाला अर्थात “नाशवान”, अर्थात जिसका नष्ट होना निश्चित है और “दुखरूप”, अर्थात लोभ- मोह- तृष्णाएँ है।। ( श्रीमद्भगवत, अध्याय- 15, श्लोक- 01)
— इसलिए इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर ही नित्य- निरंजन, यह सत्य को अनन्य भाव से प्रेमपूर्वक निरन्तर चिंतन करनेवाला ही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।।


